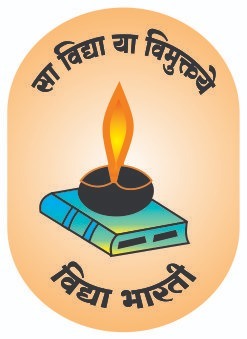विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान
- विद्या भारती राजस्थान "सेवाधाम परिसर " जयपुर राजस्थान
विद्या भारती परिचय
विद्या भारती एक परिचय
विद्या भारती एक परिचय
विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, विश्व के सबसे बड़े गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के रूप में 13000 से ज्यादा विद्यालयों, 13000 से अधिक संस्कार केन्द्रों एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयों के रूप में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में 1.5 लाख प्रशिक्षित आचार्य/दीदी, 3 लाख शिक्षाविद् मिलकर 35 लाख विद्यार्थी भैया-बहिनों को संस्कार युक्त शिक्षा दे रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा पूर्व छात्र समाज जीवन के हर क्षेत्र में पवित्र भाव से श्रेष्ठ नागरिक के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।
1952 में गोरखपुर (उत्तरप्रदेश) से कुछ शिशुओं के साथ सरस्वती शिशु मंदिर से कार्य प्रारम्भ कर आज विद्या भारती ने यह विराट स्वरूप प्राप्त किया है। भारत के प्राचीन एवं सनातन वाङ्गमय वेद, उपनिषद, पुराण, ऋषियों एवं आचायों के द्वारा सुविचारित शिक्षा के सत्य स्वरूप को ग्रहण कर विद्या भारती ने शिक्षा जगत में अपना यह स्वरूप प्राप्त किया है। शिक्षा को राष्ट्र निर्माण और प्रगति का एकमेव प्रभावी साधन मानते हुए संस्कारों की शिक्षा, बालकों के सर्वांगीण विकास की शिक्षा एवं सामाजिक चेतना का केन्द्र बन कर "वसुधैव कुटुम्बकम्" का भाव जागृत करने का कार्य विद्या भारती कर रही है।
सचरित्र, संस्कारों, वसुधैव कुटुम्बकम् एवं कृणवन्तो विश्वमार्यम् जैसे सद्गुणों की जननी इस भारतभूमि में ही आज युवकों का चरित्र पतन सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। अपने देश के गौरव को विस्मृत कर, स्वाभिमान शून्य हो, पाश्चात्य विकृतियों की ओर उनका रूझान स्पष्ट दिखाई देता है। इसका मूल कारण सुयोग्य शिक्षा का नितान्त अभाव मात्र ही है। इस अभाव की पूर्ति करने हेतु ही विद्या भारती का शुभारम्भ हुआ। बालक के हृदय में सद्गुण और संस्कार विकसित करके उसका नाता देश की माटी और पूर्वजों से जोड़कर उसमें समाज के प्रति अपनत्व और राष्ट्रभक्ति का उद्दात भाव विकसित करने के उद्देश्य से श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण एवं उनके माध्यम से राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करना ही विद्या भारती का लक्ष्य है।


राष्ट्रीय शिक्षा की पहली और सर्वोपरि व्याख्या है कि वह राष्ट्रीय आदर्शों का ज्ञान व संस्कार देने वाली शिक्षा है। परन्तु हमें याद रखना चाहिए कि शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य ‘सहानुभूति एवं विवेक बुद्धि का उदात्तीकरण’ है। विदेशी प्र्रणालियों के द्वारा इस लक्ष्य पर पहुँचना प्रायः संभव नहीं होता।
भगिनी निवेदिता

शिक्षा का अधिकतम लाभ तभी उठाया जा सकता है, जब उसे राष्ट्रीय चरित्र एवं स्वरूप में ढाल दिया जाये। वस्तुतः शिक्षा के स्वरूप को इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिय कि वह उन प्राकृतिक बन्धनों को, जो भारतीयों को एक सूत्र में बांधते हैं, और अधिक दृढ़ बनाये एवं उनमें समान राष्ट्रीयता का विकास करें।
महर्षि दयानन्द सरस्वती

शिक्षा का अर्थ है - मनुष्य को जीवन के अन्तिम लक्ष्य की ओर उन्मुख करना, तैयार कना। इस अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आवश्यक है कि मनुष्य में अनेक प्रकार के सद्गुण हों। ये सद्गुण सहसा नहीं आएँगे। इनके लिये प्रयत्न करना होगा। इसलिए इन गुणों के संस्कार बचपन से ही अपने जीवन में करते रहने की आवश्यकता है।
श्री गुरुजी

सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही है। सारे प्रशिक्षणों का अन्तिम ध्येय मनुष्य का विकास करना ही है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। शिक्षा मनुष्य में अन्तर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करने में सक्षम है।
स्वामी विवेकानन्द

छात्रों को केवल सैद्धान्तिक शिक्षा देकर ही हमें सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए। हमें विभिन्न उद्योगों एवं कलाओं की शिक्षा देने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार बच्चों की उदार एवं विस्तृत शिक्षा की ही व्यवस्था नहीं होगी, अपितु साथ ही साथ उनका बौद्धिक विकास भी होगा।